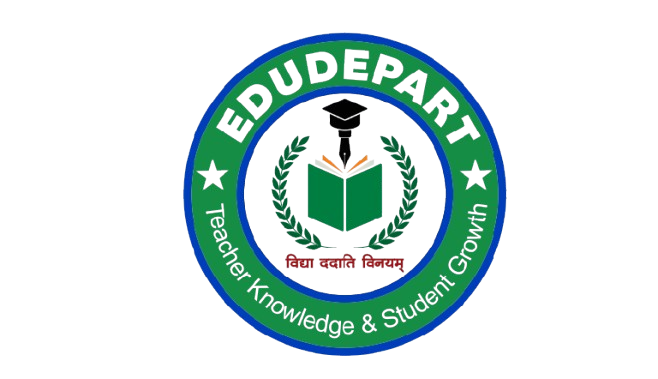| आचार्य मम्मट | काव्यप्रकाश | लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी | – काव्य के लक्षण: शब्द और अर्थ का सौन्दर्य। – अलंकार, ध्वनि, गुण, दोष, रस आदि का समन्वित विवेचन। – ध्वनि सिद्धांत का समर्थन। | संस्कृत काव्यशास्त्र का सर्वाधिक लोकप्रिय और अध्ययन हेतु मान्य ग्रंथ। |
| क्षेमेन्द्र | कविकल्पद्रुम, सुवृत्ततिलक, औचित्यविचारचर्चा | लगभग 11वीं शताब्दी | – औचित्य (समुचित सामंजस्य) को काव्य का प्राण माना। – भाषा, विषय, पात्र, स्थान, काल, भाव आदि में औचित्य पर बल। | सरल, व्यावहारिक दृष्टिकोण; कवियों को रचनात्मक मार्गदर्शन। |
| विश्वनाथ | साहित्यदर्पण | लगभग 14वीं शताब्दी | – रस को काव्य का आत्मा माना। – रस-सिद्धांत का विस्तृत प्रतिपादन। – संक्षेप में संपूर्ण काव्यशास्त्र का विवेचन। | स्पष्ट, सरस और संगठित शैली; हिंदी कवि आचार्यों पर भी प्रभाव। |
| भरत मुनि | नाट्यशास्त्र | लगभग 2वीं शताब्दी ई.पू. – 2वीं शताब्दी ई. | – रस-सिद्धांत का प्रारंभिक प्रतिपादन। – नाट्यकला, अभिनय, संगीत, छंद आदि का आधारभूत ग्रंथ। | संस्कृत नाट्यकला का विश्वकोश; रस के 8 (बाद में 9) प्रकार। |
| आनन्दवर्धन | ध्वन्यालोक | 9वीं शताब्दी | – ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन। – काव्य की आत्मा ध्वनि (अर्थ का सूक्ष्म संकेत) मानी। | अभिनवगुप्त ने इसका विस्तृत व्याख्यान किया। |
| भामह | काव्यालंकार | लगभग 7वीं शताब्दी | – काव्य में अलंकार को प्रधानता। – शब्द और अर्थ का सुंदर योग काव्य का लक्षण। | अलंकारवादी परंपरा के प्रमुख आचार्य। |
| दंडी | काव्यादर्श | लगभग 7वीं शताब्दी | – शब्द और अर्थ दोनों में शुद्धि पर बल। – गुण और दोष का विस्तार से विवेचन। | भामह के समकालीन, परन्तु दृष्टिकोण भिन्न। |