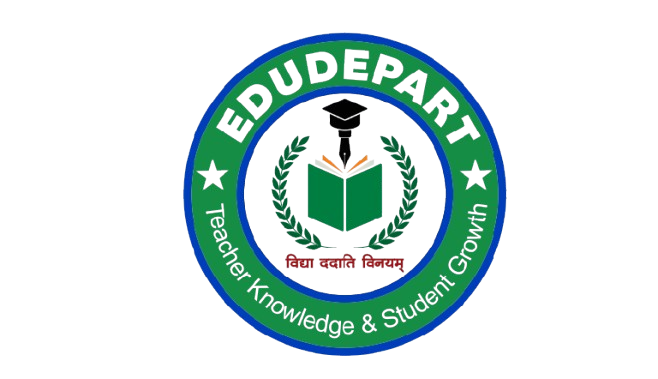मनुष्य के नेत्र की विशालन क्षमता 0-1 मि. मी. होती है। यह औसतन लगभग 300 से. मी. से 600 से. मी. (20 फुट) तक की वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन यह सामान्य गुण कभी-कभी नेत्र में सामान्य या गंभीर विकारों के कारण परिवर्तित हो जाता है।
नेत्र के विकार
नेत्र के प्रमुख विकार निम्नांकित हैं-
1. निकट दृष्टि दोष (Myopia or Near Sighteness)-
यह दोष नेत्र गोलक के आमाप के बढ़ जाने अर्थात् लेंस अथवा कॉर्निया की सतह के अधिक उत्तल हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। इस नेत्र-विकार में व्यक्ति पास की वस्तुओं को साफ लेकिन दूर की वस्तुओं को धुँधला देखता है। इस रोग में दूर की वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणे रेटिना के पहले ही बिम्ब (Image) बना देती हैं। इस रोग के निवारण हेतु अवतल लेंस (Concave lens) का चश्मा (Spect) पहना जाता है।
2. दूर दृष्टि दोष (Far-sighteness or Hypermetropia)
यह नेत्र विकार आँख के गोलक के छोटा हो जाने अथवा कॉर्निया के चपटा हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। इस नेत्र विकार में मनुष्य को दूर की वस्तुएँ साफ लेकिन पास की वस्तुएँ धुँधली दिखाई देने लगती हैं। इसे दूर करने के लिए चिकित्सक उत्तल लेंस (Convex lens) का चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। इस विकार में पास की वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणे रेटिना के चर्तित पीछे फोकस होती है जिससे वस्तु धुँधली दिखाई पड़ती है।
3. कॉन्जक्टिवाइटिस (Conjuctivitis)-
यह रोग आँखों में अत्रण के कारण होती है। इससे आँखे लाल हो जाती है तथा एवं खुजली होने लगती है। कभी-कभी ज्यादा संक्रमण के करण आँखों से पानी गिरने लगता है। सोकर उठने पर नेत्र के एक-दूसरे से चिपक जाती हैं। व्यक्तिगत सफाई Personal hygeine) तथा उपयुक्त नेत्र तरल मलहम (Eye (up) के उपयोग से यह रोग ठीक हो जाता है।
4. जीरोप्यैल्मिया (Xeropthalmia) –
विटामिन A की कमी यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में कॉन्जक्टिवा Conjuctiva) में किरैटिन का जमाव हो जाता है जिसके कारण पुष्टि दोष के रूप धुँधलापन युक्त दृष्टि हो जाती है।
5. भेंगापन (Strabismus)-
नेत्र गोलक को नेत्र-कोटर में आधे रखने का कार्य करने वाली छह कंकाली पेशियों में से यदि कोई पेशी संकुचित हो जाती है या फैल जाती है तो इसके कारण नेत्र गोलक नेत्र कोटर में एक ओर झुक जाती है, इसी विकार को भेंगापन की संज्ञा दी जाती है।
6. मोतियाबिंद (Catracts)-
इस विकार में लेंस चपटा, घना (Opaque) तथा अपारदर्शक हो जाता है, जिसके कारण चीजें धुँधली दिखने लगती हैं। इस विकार से मुक्ति के लिए आपरेशन से लेंस को पृथक्कृत कर इसके स्थान पर नया लेंस या चश्मा लगाना उचित रहता है। यह रोग बढ़ती उम्र के साथ आम विकार के रूप में आजकल देखने को मिल रहा है।
7. कालामोतिया (Glucoma)-
नेत्र गोलक स्थिति विभिन्न वेश्मों का द्रव नेत्र के हिस्सों या अंगों को अपने-अपने स्थानों पर साधे रखता है। नेत्र गोलक के वेश्मों के द्रव सिलियरी काय द्वारा स्रावित होकर नेत्र के कोष में एक नाल श्लीम के (Canal of Schlemn) द्वारा रिसता रहता है तथा एक शिरा द्वारा पुनः वापस चला जाता है। किसी कारणवश यदि श्लीम के नाल में अवरोध पैदा होता है तो यह द्रव वापस नहीं जा पाता है एवं नेत्र गोलक का दबाव बढ़ जाता है। इसके कारण रेटिना को हानि पहुँचती है जिससे अंततः देखने की क्षमता पूर्णतः समाप्त हो जाती है।
8. रेटिना पृथक्करण (Retina detachment)-
कोरॉयड (Choroid) से रेटिना की कोशिकायें पोषण प्राप्त करती हैं। रेटिना का कोई अंश जब कोरॉयड से अलग हो जाता है तो उसे पोषक पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण नेत्र के देखने की शक्ति समाप्त हो जाती है। लेंस एवं रेटिना के बीच स्थित या पारदर्शक सान्द्र द्रव के संकुचन से रेटिना पर दबाव पड़ता है, के किसी कारणवश यह स्थिति उत्पन्न होती है, तो कभी-कभी त्र रेटिना का अंश टूट जाता है एवं इस स्थान से द्रव रेटिना एवं ई कोरॉयड के बीच चला जाता है, जिससे रेटिना कोरॉइड से – पृथक्कृत हो जाता है। सर्जरी तथा औषधियों की सहायता से रेटिना के छिद्र से द्रव का जाना बंद करके एवं रेटिना तथा नी कोरॉयड के बीच संचित द्रव को निकालकर रेटिना को पुनः उपयुक्त स्थान में लाया जाता है।